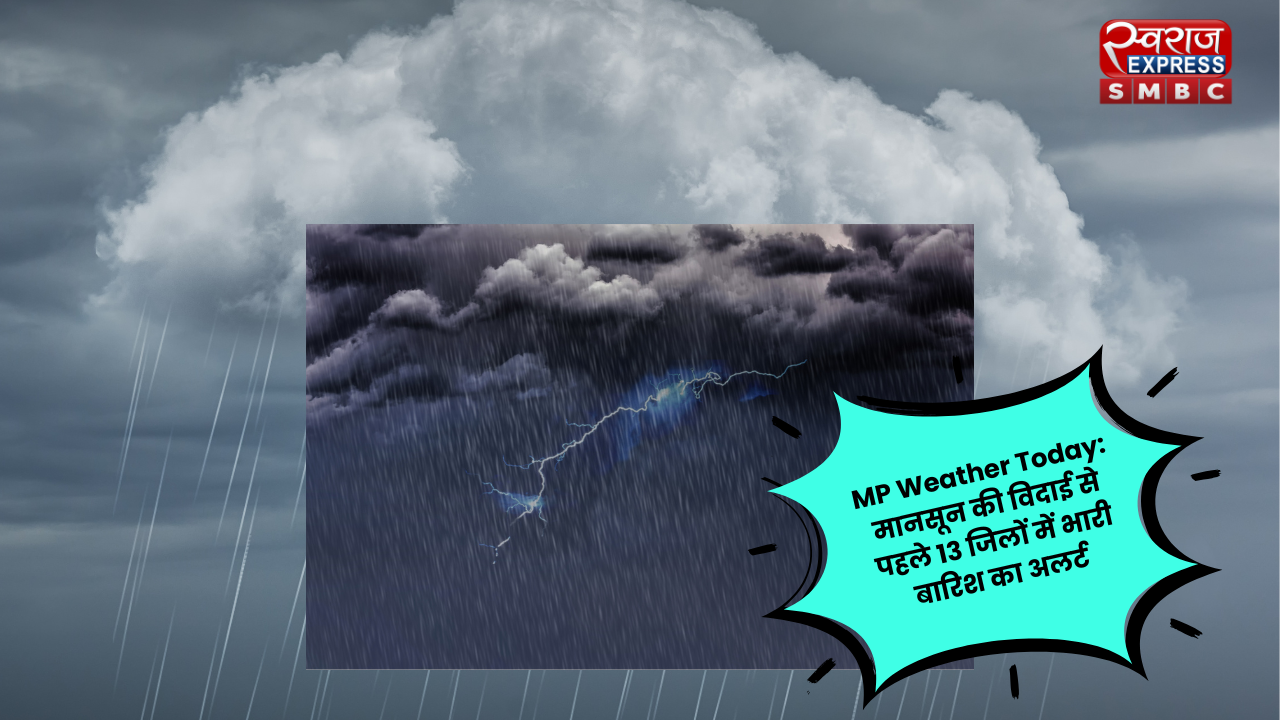Sep 19, 2016
रेटिंग 4 स्टार
कलाकार: अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ती कुल्हारी, एंड्रिया तरिआंग, अंगद बेदी, पीयूष मिश्रा, धृतमान चटर्जी, देबांग, राहुल टंडन, विनोद नागपाल, तुषार पांडे, ममता शंकर
निर्देशक: अनिरुद्ध राय चौधरी
निर्माता: रश्मी शर्मा, शुजीत सरकार
लेखक-पटकथा: रितेश शाह
संगीत: शांतनु मोइत्रा, फैजा मुजाहिद, अनुपम रॉय
अदालत में जिरह के दौरान एक वकील एक लड़की को कॉलर्गल ठहराने पर तुला है। वो बार-बार कह रहा है कि तुमने पैसे लिए हैं, तुमने पैसे लिए हैं, लिए हैं, लिए हैं, लिए हैं...मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम इस धंधे में कब से हो?
कटघरे में खड़ी वो लड़की जिसकी उम्र करीब 35 साल होगी, आखिरकार टूट जाती है और मान लेती है उसने पैसे लिए। लेकिन इससे क्या बदल जाएगा? क्या वो सच बदल जाएगा जो अदालत के सामने अब तक नहीं आया है? या इससे किसी लड़के को एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर मनचाही जगह छूने का अधिकार मिल जाएगा? प्रश्नवाचक मुद्रा में ये दृश्य एक चाबुक की तरह लगता है जिसकी मार से शरीर आहत तो होता है लेकिन आह की आवाज नहीं आती।
बतौर निर्माता और क्रीएटिव प्रोड्यूसर शुजीत सरकार की इस फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध राय चौधरी ने किया है, जिन्हें फिल्म 'अरुनानन' (2006) और 'अन्तहीन' (2008) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये उनकी पहली हिन्दी फिल्म है। फिल्म के लेखक रितेश शाह हैं, जिन्होंने इससे पहले 'मदारी', 'तीन', 'रॉकी हैंडसम' (2015) और 'बी.ए.पास' (2013) जैसी फिल्में लिखी हैं। बाकी अभिनय करने वाले कलाकारों से दर्शक भलि भांति परिचित (कीर्ती और एंड्रिया को छोड़ कर) होंगे ही।
यहां फिल्म के निर्देशक और लेखक के कार्यों पर जोर इसलिए भी कि ये फिल्म देख कर ये खयाल आता है कि परदे पर आखिर इस कंटेंट को लाने वाले कौन लोग हैं। इतनी विश्वस्नीयता और परिपक्वता के साथ एक उद्देश्यपूर्ण फिल्म बनाने में आखिर कौन-सी चीज लगती है? दिल्ली जैसे महानगर के लिए ये मौजू विषय जरूर है लेकिन इसकी विषय-वस्तु कोई नई नहीं है। फिर भी ये फिल्म पूरे सवा दो घंटे तक कैसे बेचैन-सा करे रखती है। आखिर क्या वजह है इस बेचैनी और रह रहकर होने वाली घुटन की?
ये कहानी है दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाली तीन युवतियों की। मीनल अरोड़ा (तापसी पन्नू), फलक अली (कीर्ती कुल्हारी) और एंड्रिया (एंड्रिया तरिआंग) कामकाजी युवतियां हैं और तीनों एक साथ एक किराए के घर में रहती हैं। एक दिन सूरजकुंड में एक पार्टी में इनकी मुलाकात राजवीर सिंह (अंगद बेदी) और उसके दोस्तों रौनक उर्फ डिम्पी (राहुल टंडन) और विश्वा (तुषार पांडे) से होती है। ये सभी मिल कर खाना-पीना खाते हैं, मौज-मस्ती करते हैं और अचानक इनमें लड़ाई हो जाती है। मीनल, राजवीर के सिर पर एक बोतल से वार करती है, जिससे वह घायल हो अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी आंख जाते-जाते बचती है। इधर, इस घटना से घबराई ये तीनों युवतियां देर रात अपने घर आ जाती हैं और किसी को कुछ नहीं बतातीं।
घटना के एक-दो दिन बाद राजवीर और उसके दोस्त इन तीनों युवतियों से बदला लेने की नीयत से इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तीनों घबरा जाती हैं और मदद के लिए पुलिस के पास जाती हैं जहां से इन्हें 'टरका' दिया जाता है। राजवीर चूंकि एक रसूखदार परिवार से है तो वह पुलिस वाली बात गंभीरता से लेता है और मामले को कुछ ऐसे घुमाता है कि पुलिस उल्टा इन युवतियों को गिरफ्तार कर लेती है।
मीनल को राजवीर की हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस उठा कर ले जाती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है जहां इन तीनों युवतियों का केस शहर का एक नामी और काबिल वकील दीपक सहगल (अमिताभ बच्चन) लड़ता है। पहली पेशी में ही राजवीर का वकील प्रशांत (पीयूष मिश्रा) अदालत को ये विश्वास दिलाने में जुट जाता है कि ये तीनों युवतियां दरअसल कॉलर्गल हैं और घटना वाली रात अपनी मर्जी से पैसों के लालच में राजवीर और उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाने की गरज से कमरे में गईं थीं।
दिल्ली जैसा शहर जहां अधिकतर रसूखदार या गैर-रसूखदार छोटी-छोटी बात पर ये कहते नजर आते हैं कि 'तुझे पता है कि मैं कौन हूं', 'मेरा बाप कौन है', में यह कहानी कोई नई नहीं लगती। और शायद ये कहानी किसी ऐसे केस के बारे में है भी नहीं।
दरअसल ये प्रस्तुतिकरण है एक मानसिकता का, जहां कामकाजी लड़कियों-युवतियों के चरित्र का अंदाजा उनके कपड़ों और उन्मुक्तता से लगाया जाता है। एक ही शहर में रह कर कोई लड़की अपने माता-पिता के घर से अलग हो कर कैसे रह सकती है? अगर वो ऐसा करती है तो वह चरित्रहीन है। और पूर्वोत्तर राज्य से आई कोई लड़की। वो तो होती ही ऐसी हैं? क्या वाकई...
ये कुछ धारणाएं हैं जिन पर बड़े ही प्रभावशाली और असरकार ढंग से फिल्म में एक बड़ा प्रहार किया गया है। फिल्म की पटकथा बेहद विश्वस्नीय ढंग से लिखी गई है। लगता ही नहीं कि ये कोई फिल्म है। यहां बनावटीपन की कोई गुंजाइश नहीं है। किरदार इतने असल लगते हैं कि उन पर विश्वास करने का मन करता है। फिर चाहे वो मकान मालिक कस्तूरी लाल (विनोद नागपाल) या फिर जज सत्यजीत दत्त (धृतमान चटर्जी)। एसएचओ सरला देवी का किरदार इतना असल और प्रभावी लगता है कि मानो आप इस किरदार से कई बार मिल चुके हैं।
अदालत के एक सीन में सरला को दीपक सहगल सुपरवुमन संबोधित करता है। इसके बाद का करीब पांच मिनट का सीन सन्न और सोच पैदा करने वाला है जो हमारी पुलिस की कार्यशैली की पोल खोलता है।
ऐसे ही एक अन्य सीन में दीपक का राजवीर को पेंट की जेब से हाथ निकाल कर खड़ा होने की सलाह देने वाला दृश्य समाज में 'इलीट क्लास' की अकड़ और सभ्यता की तरफ इशारा करता है।
इंटरवल के बाद की पूरी फिल्म कोर्टरूम ड्रामा है, जिसके लगभग हर सीन में एक जरूरत झलकती है। वो जरूरत जो आज हर सभ्य को है। सोच बदलने की जरूरत, तहजीब की जरूरत और महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म कोई नई बात नहीं दिखाती। ऐसी बातें आए दिन आप टीवी डिबेट या किसी अखबार के संपादकीय में पढ़ते होंगे। लेकिन इन्हीं सब बातों को एक प्रभावशाली ढंग से कहने का एक तरीका ये भी हो सकती है, ये फिल्म बस यही दर्शाती है। निर्देशक ने इन तमाम बातों को कहने के लिए बेहद सहज तरीका अपनाया है। उन्होंने यथासंभव स्थिति को वैसे ही दिखाया और बयां किया है, जो असल में हमारे साथ हो सकता है। इसीलिए फिल्म के अधिकतर सीन बेचैन करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, कई जगह तो घुटन भी पैदा करते हैं।
अभिनय की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर चौंकाया है। ऐसे कई बार लगा कि ये भूमिका शायद वही कर सकते थे। तापसी पन्नू, कीर्ती और एंड्रिया के अलावा पीयूष मिश्रा ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। राजवीर के किरदार में अंगद बेदी से आपको नफरत सी होने लगती है। मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और उसे ढंग से प्रस्तुत भी किया है।
ये फिल्म हर महिला-पुरुष के लिए जरूरी है। हर समाज के लिए जरूरी है। खासतौर से उनके लिए जो बलात्कार और छोड़खानी की घटनाओं के लिए महिलाओं के कपड़ों और उनकी उन्कुक्तता को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस फिल्म के माध्यम से ये जानना भी जरूरी है कि आखिर समाज को क्यों अब लड़कियों के बजाए अपने लड़कों की रक्षा करनी चाहिए...